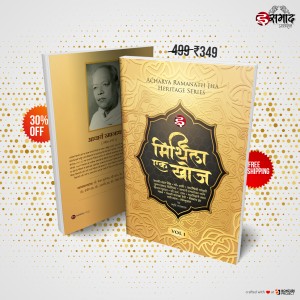किसी भी फिल्म में एक हीरो होता है, कैमरा जिसके पीछे पूरी फिल्म में भागता रहता है। ठीक उसी तरह क्रिकेट का मुख्य किरदार होती है गेंद। जिधर गेंद उधर-उधर खिलाड़ी। अंपायर से लेकर बल्लेबाज, यहां तक कि स्टेडियम में बैठे दर्शक भी उसी गेंद पर नजर गड़ाए रखते हैं। कैमरों के लेंस भी उसी गेंद को कैद करने को आतुर होते हैं, चूकीं इस खेल की हीरोइन गेंद है इसलिए उसके लुक में भी बदलाव होते रहे हैं।
1877 में लाल गेंद से शुरू हुआ टेस्ट क्रिकेट का सफर अपनी गुलाबी मंजिल तक तो पहुंच चुका है, लेकिन सफर अब भी जारी है। टीम इंडिया डे-नाइट टेस्ट में प्रवेश कर रही है। जिसमें गुलाबी गेंद इस्तेमाल होगी। भारतीय टीम पहली बार एक पिच पर पांच दिन डे-नाइट क्रिकेट खेलेगी और वह पिच होगी ईडन गार्डंस की।
डे-नाइट टेस्ट की शुरुआत 27 नवंबर 2015 को हो गई थी। एडीलेड की दूधिया रोशनी में आमने-सामने थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत-बांग्लादेश के अलावा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सभी प्रमुख देश डे-नाइट टेस्ट खेल चुके हैं। डे-नाइट टेस्ट को लेकर तमाम बातें चर्चा में हैं, लेकिन सबसे अधिक जो सुर्खियों में है, वह गुलाबी गेंद।
पहली पिंक बॉल
पहली गुलाबी गेंद का निर्माण ऑस्ट्रेलिया की बॉल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी कूकाबूरा ने किया था। कूकाबूरा ने कई साल तक इस नई पिंक बॉल को लेकर परीक्षण किया तब जाकर एक बेहतरीन गुलाबी गेंद बन पाई। पहली पिंक बॉल तो 10 साल पहले बन गई थी, मगर इसकी टेस्टिंग करते-करते पांच-छह साल और लग गए। आखिरकार 2015 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले डे-नाइट टेस्ट में पिंक बॉल से खेला गया। इसके बाद से इस नई गेंद का सफर बढ़ चला।
गुलाबी रंग ही क्यों?
टेस्ट क्रिकेट सफेद जर्सी में खेला जाता है, तो इसलिए उसमें लाल रंग की गेंद का इस्तेमाल होता है, ताकि गेंद आसानी से नजर आए। उसी तरह वन-डे रंगीन कपड़ों में होता है, ऐसे में उसमें सफेद गेंद इस्तेमाल होती है। अब डे-नाइट टेस्ट में गुलाबी रंग की गेंद का ही क्यों इस्तेमाल होता है, यह सवाल तमाम क्रिकेट फैंस के जेहन में उभर रहा होगा।
इस पिंक के पीछे की वजह बताई थी कूकाबूरा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रेट एलियट ने, एलियट ने कहा था कि शुरुआत में हमने कई तरह के रंगों का इस्तेमाल किया, जैसे कि येलो और ऑरेंज, लेकिन इन रंगों की गेंदों में सबसे बड़ी समस्या थी कि, यह कैमरा फ्रेंडली नहीं थी। दरअसल मैच कवर कर रहे कैमरामैन ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा था कि ऑरेंज कलर को कैमरा के लिए कैप्चर कर पाना काफी मुश्किल होता है, यह गेंद दिखाई नहीं देती। इसके बाद सबकी सहमति से पिंक कलर को चुना गया।
वन-डे वाली सफेद क्यों नहीं ?
वन-डे में दो नई गेंदें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि सफेद गेंद का रंग जल्दी नहीं खराब हो और दूधिया रोशनी में इसे आसानी से देखा जा सके। वहीं टेस्ट क्रिकेट में लगातार 80 ओवर का मैच होने के बाद ही गेंद बदली जाती है। वन-डे की एक पारी के बाद ही सफेद गेंद का रंग भूरा पड़ने लगता है, वहीं 80 ओवर्स तक तो इसका रंग गहरा भूरा हो जाएगा और पिच भी भूरी होती है।
यानी बल्लेबाजों को नहीं बल्कि फील्डर्स को भी इससे खासी परेशानी होगी। इसके साथ ही टेस्ट भले ही डे-नाइट हो रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के कपड़ों का रंग सफेद ही रहेगा। यानी सफेद गेंद से इस टेस्ट के खेले जाने का कोई भी सवाल नहीं पैदा होता।
16 तरह के पिंक शेड्स में चुना गया एक
एक बार गुलाबी रंग पर मुहर लगने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि पिंक में भी कैसा पिंक कलर होगा। इसके लिए करीब पिंक के 16 शेड्स ट्राई किए गए। एलियट बताते हैं, ‘हमने 16 तरह के पिंक कलर का परीक्षण किया और हर बार उसमें बदलाव देखने को मिला। अंत में एक आयडल शेड को सलेक्ट किया गया जिसकी बनी गेंद अब डे-नाइट टेस्ट मैच में इस्तेमाल होती है।
रंग के फाइनल हो जाने के बाद कंपनी के समाने बड़ी समस्या ये थी कि इसकी सिलाई किस रंग के धागे से की जाए। इसके लिए भी तमाम प्रयोग किए गए। कूकाबूरा कंपनी ने पिंक बॉल की सिलाई सबसे पहले काले रंग के धागे से की थी। इसके बाद हरा रंग इस्तेमाल हुआ, फिर सफेद कलर के धागे का प्रयोग हुआ। अंत में हरे रंग की सिलाई पर सबकी सहमति बनी, लेकिन टीम इंडिया जिस कंपनी की बनाई गुलाबी गेंद से खेलेगी उसकी सिलाई काले रंग के धागे से हुई है।
निर्माण प्रक्रिया
रेड और पिंक बॉल की निर्माण प्रक्रिया में कोई बड़ा अंतर नहीं है। अंदर से यह दोनों गेंदें एक तरह की होती है बस अंतर है तो इनकी कलर कोटिंग का। बाकि बाउंस, हार्डनेस और परफॉर्मेंस के लिहाज से यह दोनों गेंद एक जैसी हैं। रेड बॉल में लेदर को लाल रंग से रंग कर उसकी घिसाई की जाती है जबकि गुलाबी गेंद में गुलाबी, लेकिन फिनिशिंग के दौरान पिंक बॉल पर रंग की एक और परत चढ़ाई जाती है। इसकी वजह से गेंद का रंग कुछ अधिक अंतराल तक चमकीला बना रहा है। यानी शाइन बरकरार रहती है।
कूकाबूरा और एसजी की गेंद में फर्क
एसजी गेंदों में एक व्यापक सीम होती है जो एक साथ करीब होती है, क्योंकि उन्हें बनाने के लिए टिकर धागे का उपयोग किया जाता है। यहां तक कि अब गेंदें हस्तनिर्मित हैं और उनके पास सीम है जो खेल के एक दिन बाद भी अच्छी स्थिति में रहती है। ये गेंदें व्यापक सीम के कारण स्पिनरों के लिए मददगार होती हैं। चमक खत्म होने के बाद, यह गेंदबाज को 40 ओवर तक रिवर्स स्विंग कराने में मदद करता है।
कूकाबूरा की गेंद कम सीम प्रदान करती है, लेकिन गेंद को 30 ओवर तक स्विंग करने में मदद करती है। स्पिन गेंदबाजों को इन गेंदों से बहुत मदद नहीं मिलती है, और जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, बल्लेबाज के लिए बिना ज्यादा मुश्किल के शॉट खेलना आसान हो जाता है।